*आध्यात्मिक क्रांति का जनक श्रमण जैन चातुर्मास*
- प्रो. फूलचन्द जैन प्रेमी, वाराणसी
अपने भारत देश में वैदिक एवं श्रमण – ये दोनों संस्कृतियाँ प्राचीन काल से ही समृद्ध रही हैं, और इन दोनों में ही चातुर्मास का अत्यधिक महत्त्व है । श्रमण जैन परंपरा में तो चातुर्मास को चार मास के लंबे महापर्व के रूप में आयोजित किए जाने का विधान हैं ।
वर्षाकाल के आरंभ से ही चार माह के लिए एक ही स्थान पर लंबे प्रवास में साधु-साध्वियों के ज्ञान, ध्यान और संयम साधना का लाभ समाज को प्राप्त होता है । चौबीसवें एवं अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के अनेक चातुर्मास का विवरण हमें प्राकृत जैनागमों से प्राप्त होता है । इस चातुर्मास काल में आष्टान्हिक पर्व, रक्षाबंधन, पर्युषण-दशलक्षण सांवत्सरिक महापर्व, क्षमावाणी तथा तीर्थंकरों के पञ्च कल्याणकों जैसे अनेक पर्व भी मनाए जाते हैं ।
वस्तुतः यत्र-तत्र गमनागमन रूप विहारचर्या श्रमण जीवन की एक अनिवार्य एवं महत्त्वपूर्ण चर्या है । इसीलिए श्रमण को अनियत विहारी कहा जाता है । क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र (४/६) में कहा है कि “भारण्ड-पक्खीव चारेsप्पमत्तो” – अर्थात् श्रमण को भारण्ड पक्षी की तरह ग्रामानुग्राम आदि क्षेत्रों में अनासक्त भाव से निरंतर विचरण करते हुए अपनी साधना में लीन रहना चाहिए । इससे सम्यग्दर्शन की शुद्धि, स्थितिकरण, रत्नत्रय की भावना, शास्त्राभ्यास, शास्त्र कौशल, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना के साथ ही आवश्यकतानुसार समाधिमरण के योग्य क्षेत्रों का अन्वेषण जैसे सहज लाभ इस अनियत विहारचर्या से प्राप्त हो जाते हैं ।
किन्तु वर्षाकाल के चातुर्मास में चार माह तक निरंतर एक स्थान पर प्रवास करने का भी अनिवार्य शास्त्रीय प्रावधान है ।
चातुर्मास की अवधारणा -
श्रमण जैन परम्परा में चातुर्मास अर्थात् वर्षावास, जैनमुनिचर्या का आचारगत अनिवार्य और महत्त्वपूर्ण योग है। इसे वर्षायोग,वर्षावास अथवा चातुर्मास भी कहा जाता है । श्रमण के आचेलक्य आदि दस स्थितिकल्पों में अन्तिम पर्युषणा कल्प है । जिसके अनुसार वर्षा काल के चार महीने भ्रमण अर्थात् आवागमन,विहार आदिका त्याग करके एक स्थान पर रहने का विधान है। वर्ष के बारह महीनों को मौसम की दृष्टि से प्रमुख तीन भागों में विभाजित किया गया है-
ग्रीष्म– चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ ।
वर्षा – श्रावण, भाद्रपद, आश्विन तथा कार्तिक ।
शीत –मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा फाल्गुन ।
यद्यपि ये तीनों ही विभाजन चार-चार माह के हैं, किन्तु वर्षाकाल के चार महीनों का एकत्र नाम चातुर्मास, वर्षावास आदि रूप में प्रसिद्ध है ।
श्वेताम्बर जैन आगम परम्परा में “पर्युषणा कल्प” नाम से वर्षावास का वर्णन प्राप्त होता है । बृहत्कल्पभाष्य में इसे 'संवत्सर' कहा गया है ।वस्तुतःवर्तमान युग में पर्यावरण बहुत कुछ बदल गया है । अब न तो वर्षाकाल में पूरीतरह वर्षा का भरोसा रहता है,न शीतकाल में भरपूर ठण्ड का और न इसी तरह अन्य ऋतुओं का ।
वर्तमान युग में तो गर्मी के बढ़ते प्रकोप से सभी त्रस्त रहते हैं । पर्यावरण प्रदूषण का असर सर्वत्र देखा जा सकता है ।किन्तु अब से सात – आठ दशक पूर्व तक ऐसी स्थिति नहीं थी ।पहले आवागमन के आज जैसे साधन भी नहीं थे । बड़ी-बड़ी सड़कों का जाल नहीं था । वर्षाकाल में प्रायः सदा आकाश मण्डल में घटाएं छायी रहती थीं तथा प्रायः वर्षा भी निरन्तर होती रहती थी ।अतः वर्षाकाल में यत्र-तत्र भ्रमण या विहार के मार्ग रुक जाते हैं, नदी, नाले उमड़ पड़ते हैं । वनस्पतिकाय आदि हरित्काय मार्गों और मैदानों में फैल जाती है । सूक्ष्म-स्थूल जीव-जन्तु उत्पन्न हो जाते हैं । अतः छोटे -बड़े किसी भी प्रकार के जीवों को हमारे चलने फिरने से कष्ट न पहुंचे,उनकी विराधना और आत्म विराधना (घात) से बचने के लिए श्रमण धर्म में वर्षा काल में वर्षायोग धारण,इस चातुर्मास में एकत्र-वास का विधान किया गया है ।
यही समय एक स्थान पर स्थिर रहने का सबसे उत्कृष्ट समय होता है । श्रमण और श्रावक-दोनों के लिए इस चातुर्मास का धार्मिक तथा आध्यात्मिक और संयम साधना के विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्व है ।
इसीलिए श्रमण या उनके संघ के चातुर्मास (वर्षा योग) को श्रावक उसी प्रकार प्रिय और हितकारी अनुभव करते हैं, जिस प्रकार चकवा चन्द्रोदय को, कमल सूर्य को और मयूर मेघोदय को ।
चातुर्मास का औचित्य–
अपराजितसूरि ने भगवती आराधना की विजयोदया टीका में कहा है कि वर्षाकाल में स्थावर और जंगम सभी प्रकार के जीवों से यह पृथ्वी व्याप्त रहती है । उस समय भ्रमण करने पर महान् असंयम होता है । वर्षा और शीत वायु (झंझावात) से आत्मा की विराधना होती है । वापी आदि विविध जलाशयों में गिरने का भय रहता है । जलादि में छिपे हुए ठूठ, कण्टक आदि से अथवा जल, कीचड़ आदि से कष्ट पहुँचता है और अपना जीवन भी खतरे में पड़ सकता है ।
आचारांग में कहा है कि वर्षाकाल आ जाने पर तथा वर्षा हो जाने से मार्ग पर बहुत से प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत से बीज अंकुरित हो जाते हैं । बहुत हरियाली उत्पन्न हो जाती है। ओस और पानी बहुत स्थानों में भर जाता है । काई आदि स्थान-स्थान पर व्याप्त हो जाती है। बहुत से स्थानों पर कीचड़ या पानी से मिट्टी गीली हो जाती है । मार्ग रुक जाते हैं, मार्ग पर चला नहीं जा सकता। मार्ग सूझता नहीं है,अतः इन परिस्थितियों को देखकर मुनि को वर्षा काल में एक ग्राम से दूसरे ग्राम विहार नहीं करना चाहिए । अपितु वर्षाकाल में यथावसर प्राप्त वसति में ही संयत रहकर वर्षावास व्यतीत करें ।
बृहत्कल्पभाष्य के अनुसार वर्षावास में गमन करने से पृथ्वी,जल,तेज,वायु,वनस्पति और त्रस -- इन षट्कायिक जीवों का घात तो होता ही है, साथ ही वृक्ष की शाखा आदि सिर पर गिरने, कीचड़ में रपट जाने, नदी में बह जाने, काँटा आदि लगने के भय रहते हैं।
श्रमण जैनमुनि को प्रत्येक कार्य करते समय अहिंसा और विवेक की दृष्टि रखना अनिवार्य है । वर्षाकाल में विहार करते रहने में अनेक बाधाओं के साथ ही जीव-हिंसा की बहुलता सदा रहती है, इसीलिए वर्षाकाल चार माह तक एक स्थान पर स्थिर रहकर वर्षायोग धारण का विधान है । इस प्रकार जैन परम्परा के साथ ही प्रायः सभी भारतीय परम्पराओं के धर्मों में साधुओं को वर्षाकाल के चार माह में एक स्थान पर स्थित रहकर धर्म-साधन करने का विधान है।
चातुर्मास का समय -
सामान्यतः आषाढ़ से कार्तिक पूर्वपक्ष तक का समय वर्षा और वर्षा से उत्पन्न जीव-जीवाणुओं तथा अनन्त प्रकार के तृण, घास और जन्तुओं के पूर्ण परिपाक का समय रहता है । इसीलिए चातुर्मास (वर्षावास) की अवधि आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी की पूर्वरात्रि से आरम्भ होकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की पश्चिम रात्रि तक मानी जाती है ।
वर्षावास के समय में एक सौ बीस दिन तक एक स्थान पर रहना उत्सर्ग मार्ग है । विशेष परिस्थिति अथवा कारण होने पर अधिक और कम दिन भी ठहर सकते हैं । अर्थात् आषाढ़ शुक्ला दसमी से चातुर्मास करने वाले कार्तिक की पूर्णमासी के बाद तीस दिन तक आगे भी सकारण एक स्थान पर ठहर सकते हैं । अधिक ठहरने के प्रयोजनों में वर्षा की अधिकता, शास्त्राभ्यास, शक्ति का अभाव अथवा किसी की वैयावृत्य करना आदि हैं । आचारांग में भी कहा है कि वर्षाकाल के चार माह बीत जाने पर अवश्य विहार कर देना चाहिए, यह तो श्रमण का उत्सर्ग मार्ग है । फिर भी यदि कार्तिक मास में पुनः वर्षा हो जाए और मार्ग आवागमन के योग्य न रहे तो चातुर्मास के पश्चात् वहाँ पन्द्रह दिन और रह सकते हैं ।
समय की दृष्टि से वर्षावास के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट-- ये तीन भेदबताये हैं।इनमें सांवत्सरिक प्रतिक्रमण (भाद्रपद शुक्ला पंचमी) से कार्तिक पूर्णमासी तक सत्तर दिनों का जघन्य वर्षावास कहा जाता है । श्रावण से कार्तिक तक-चार माह का मध्यम चातुर्मास है तथा आषाढ़ से मृगसर तक छह माह का उत्कृष्ट वर्षावास कहलाता है । इसके अन्तर्गत आषाढ़ बिताकर वहीं चातुर्मास करें और मार्गशीर्ष में भी वर्षा चालू रहने पर उसे वहीं बितायें ।'
स्थानांग आगमवृत्ति में कहा है कि प्रथम प्रावृट (आषाढ़) में और पर्युषणा कल्प के द्वारा निवास करने पर विहार न किया जाए। क्योंकि पर्युषणाकल्प पूर्वक निवास करने के बाद भाद्र शुक्ला पंचमी से कार्तिक तक साधारणतः विहार नहीं किया जा सकता, किन्तु पूर्ववर्ती पचास दिनों में उपयुक्त सामग्री के अभाव में विहार कर भी सकते है ।
बृहत्कल्पभाष्य में वर्षावास समाप्त कर विहार करने योग्य समय के विषय में कहा है कि जब ईख बाड़ों के बाहर निकलने लगें, तुम्बियों में छोटे-छोटे तुंबक लग जायें, बैल शक्तिशाली दिखने लगे, गाँवों की कीचड़ सूखने लगे, रास्तों का पानी कम हो जाए, जमीन की मिट्टी कड़ी हो जाय तथा जब पथिक परदेश को गमन करने लगे तो श्रमण को भी वर्षावास की समाप्ति और अपने विहार करने का समय समझ लेना चाहिए।
चातुर्मास के योग्य स्थान -
श्रमण को वर्षायोग के धारण का उपयुक्त समय जानकर धर्म-ध्यान और चर्या आदि के अनुकूल योग्य प्रासुक स्थान पर चातुर्मास व्यतीत करना चाहिए । आचारांग आगमसूत्र में चातुर्मास योग्य स्थान के विषय में कहा है कि वर्षावास करने वाले साधु या साध्वी को उस ग्राम-नगर खेड, कवंट, मडंब, पट्टण, द्रोणमुख, आकर (खदान), निगम, आश्रय, सन्निवेश या राजधानी की स्थिति भलीभाँति जान लेनी चाहिए । जिस ग्राम-नगर यावत् राजधानी में एकान्त में स्वाध्याय करने के लिए विशाल भूमि न हो, मल-मूत्र त्याग के लिए योग्य विशाल भूमि न हो, पीठ (चौकी) फलक, शय्या एवं संस्तारक की प्राप्ति सुलभ न हो और न प्रासुक (निर्दोष) एवं एषणीय आहार-पानी हो सुलभ हो, जहाँ बहुत से श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, दरिद्र और भिखारी पहले से आए हुए हों और भी दूसरे आनेवाले हों, जिससे सभी मार्गों पर जनता की अत्यन्त भीड़ हो और साधु-साध्वी को भिक्षाटन, स्वाध्याय, शौच आदि आवश्यक कार्यों के लिए अपने स्थान से सुखपूर्वक निकलना और प्रवेश करना भी कठिन हो, स्वाध्याय आदि क्रिया भी निरुपद्रव न हो सकती हो, ऐसे ग्राम-नगर आदि में वर्षाकाल प्रारम्भ हो जाने पर भी वर्षावास व्यतीत न करे ।
प्राकृत आगम कल्पसूत्र की कल्पलता टीका के अनुसार जैन साधु -साध्वियों को चातुर्मास के योग्य स्थान में निम्नलिखित गुण होना चाहिए--जहाँ विशेष कीचड़ न हो, जीवों को अधिक उत्पत्ति न हो, पंचम समिति के सम्यक् पालन हेतु शौच-स्थल निर्दोष हो, रहने का स्थान शान्तिप्रद एवं स्वाध्याय योग्य हो, गोरस की अधिकता हो, जनसमूह भद्र हो, राजा धार्मिक वृत्ति का हो, भिक्षा सुलभ हो, श्रमण-ब्राह्मण का अपमान न होता हो । ऐसे ही अनुकूल और निरापद स्थान चातुर्मास के सर्वथा योग्य होते हैं ।
वर्षायोग ग्रहण एवं उसकी समाप्ति की विधि -
यद्यपि दूसरी सदी के वट्टकेराचार्य द्वारा रचित मूलाचार आदि प्राकृत भाषा के प्राचीन ग्रन्थों में वर्षायोग गृहण आदि की विधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं है ,किन्तु उत्तरवर्ती विद्वान् पंडित आशाधर प्रणीत ग्रन्थ अनगार धर्मामृत ग्रंथ में कहा है कि आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी की रात्रि के प्रथम पहर में पूर्व आदि चारों दिशाओं में प्रदक्षिणा क्रम से लघु चैत्यभक्ति चार बार पढ़कर सिद्धभक्ति,योगिभक्ति,पंचगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति करते हुए आचार्य आदि साधुओं को वर्षायोग ग्रहण करना चाहिए तथा कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि के पिछले पहर में इसी विधि से वर्षायोग को छोड़ना चाहिए।
आगे बताया है कि वर्षायोग के सिवाय अन्य हेमन्त आदि ऋतुओं में अर्थात् ऋतुबद्ध काल में श्रमणों का एक स्थान में एक मास तक रुकने का विधान है ।
अनगारधर्मामृत में ही आगे कहा है कि जहाँ चातुर्मास करना अभीष्ट हो, वहाँ आषाढ़ मास में वर्षायोग के स्थान पर पहुँच जाना चाहिए तथा मार्गशीर्ष महीना बीतने पर वर्षायोग के स्थान को छोड़ देना चाहिए । कितना ही प्रयोजन होने पर भी वर्षा योग के स्थान में श्रावण कृष्णा चतुर्थी तक अवश्य पहुँच जाना चाहिए। इस तिथि का उल्लंघन नहीं करना चाहिए तथा कितना ही प्रयोजन होने पर भी नहीं ।
कार्तिक शुक्ला पंचमी तक वर्षायोग के स्थान से अन्य स्थान को नहीं जाना चाहिए। यदि किसी दुर्निवार उपसर्ग आदि के कारण वर्षायोग के उक्त प्रयोग में अतिक्रम करना पड़े तो साधु को प्रायश्चित्त लेना चाहिए।
वर्षायोग धारण के विषय में श्वेताम्बर परम्परा के कल्पसूत्र आगम में कहा है कि मासकल्प से विचरते हुए निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को आषाढ़ मास की पूर्णिमा को चातुर्मास के लिए वसना कल्पता है । क्योंकि निश्चय ही वर्षाकाल में मासकल्प विहार से विचरने वाले साधुओं और साध्वियों के द्वारा एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक के जीवों को विराधना होती है।
कल्पसूत्रनिर्युक्ति में भी कहा है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा तक नियत स्थान पर पहुँचकर श्रावण कृष्ण पंचमी से वर्षावास प्रारम्भ कर देना चाहिए । उपयुक्त क्षेत्र न मिलने पर श्रावण कृष्ण दसमी से पाँच-पाँच दिन बढ़ाते-बढ़ाते भाद्र शुक्ल पंचमी तक तो निश्चित ही वर्षांवास प्रारम्भ कर देना चाहिए, फिर चाहे वृक्ष के नीचे ही क्यों न रहना पड़े । किन्तु इस तिथि का उल्लंघन नहीं होना चाहिए ।
चातुर्मास में भी विहार करने के कारण -
भगवती आराधना प्राकृत भाषा के प्राचीनग्रंथ की विजयोदया टीका में अपराजितसूरि के अनुसार वर्षायोग धारण कर लेने पर भी यदि दुर्भिक्ष पड़ जाए, महामारी फैल जाये, गाँव अथवा प्रदेश में किसी कारण से उथल-पुथल हो जाए, गच्छ का विनाश होने के निमित्त आ जाये तो देशान्तर में जा सकते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में वहाँ ठहरने से रत्नत्रयधर्म और संयम की विराधना होगी। आषाढ़ की पूर्णमासी बीतने पर प्रतिपदा आदि के दिन देशान्तर गमन कर सकते हैं । स्थानांगसूत्र प्राकृत आगम में इसके पांच कारण बताये हैं–
१. ज्ञान के लिए,
२. दर्शन के लिए,
३. चारित्र के लिए,
४. आचार्य या उपाध्याय की सल्लेखना/समाधिमरण के अवसर पर तथा
५. वर्षाक्षेत्र से बाहर रहे हुए आचार्य अथवा उपाध्याय का वैयावृत्त्य करने के लिए।
साथ ही यह भी कहा है कि निर्ग्रन्थ और साध्वियों को प्रथम प्रावृट् चातुर्मास के पूर्वकाल में ग्रामानुग्राम विहार नहीं करना चाहिए । संघ में रहकर साधना ,संयम और ज्ञानाभ्यास करना चाहिए ।
किन्तु इन पाँच कारणों से विहार किया भी जा सकता है–
१. शरीर, उपकरण आदि के अपहरण का भय होने पर,
२. दुर्भिक्ष होने पर,
३. किसी के द्वारा व्यथित किये जाने पर अथवा ग्राम से निकाल दिये जाने पर,
४. बाढ़ आ जाने पर तथा
५. अनार्यों द्वारा उपद्रुत किये जाने पर ।
इस प्रकार श्रमण के लिए चातुर्मास अर्थात् वर्षावास का समय उसी प्रकार कषायरूपी अग्नि एवं मिथ्यात्व रूपी ताप को त्याग एवं वैराग्य की शीतल धारा से तथा स्वाध्याय और ध्यान की जलवृष्टि से शान्त करने का होता है, जिस प्रकार जल के शीतलधारा बरसकर धरती की तपन शान्त करती है ।
इस तरह जैन परम्परा में चातुर्मास का धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में विकास का महत्त्व तो है ही, इससे राष्ट्रप्रेम के साथ ही व्यक्ति और समाज को एक सूत्र में पिरोने का, वैर भाव दूर करके मैत्री,सौहार्द्र एवं समरसता का वातावरण निर्मित करने का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य सिद्ध है।
प्रयुक्त संदर्भ _____
प्रस्तुत आगम प्रमाण युक्त शोध आलेख लेखक की प्रकाशित सुप्रसिद्ध कृति *मूलाचार का समीक्षात्मक अध्ययन* से लिया गया है अतः विशेष अध्ययन हेतु उसका अध्ययन करना चाहिए । यह ग्रंथ पार्श्वनाथ विद्यापीठ,वाराणसी से प्रकाशित है ।
१. मूलाचार वृत्ति १०।१८.नीं
२. मूलाचार ९।१९.
३. भ० आ० वि० टीका ४२१.
४. मूलाचार वृत्ति १०११८.
५. भ० आ० वि० टीका ४२१.
६.स्थानांग वृत्ति १०।११५. पृ० ४८५.
७. वर्षाकालस्य चतुर्षु मासेषु एकत्रैवावस्थानं भ्रमणत्यागः -भ० आ० वि० टी० ४२१, मूलाचारवृत्ति १०।१८.
_____
८. बृहत्कल्पभाष्य १।३६.
९, भगवती आरा० विजयो० टीका ४२१
१०. आचारांग सूत्र २।३।१।१११.
११. बृहत्कल्पभाष्य भाग ३ गाथा २७३६-२७३०.
१२. अनगार धर्मामृत ९।६६-६७.
१३. अनगार धर्मामृत ९।६८-६९
१४. कप्पइ निग्गंथाणं वा निग्गंथीणं वा एवं विहेणं विहाररेणं विहरमाणाणं आसाढपुण्णिमाए वासावासं वसित्तए–कल्पसूत्र : सूत्र १७ पृ० ७४ (कल्पमंजरी टीका सहित ।
१५. कल्पसूत्र निर्युक्ति गाथा १६, कल्पसूत्र चूर्णी पृ० ८९.
१६. भ. आ० वि० टीका ४२१. ४.
१७. आचारांग २।३।१।११३ पृ० १०६४.
१८. ठाणंः टिप्पण ५।६१-६२. पृ० ६२५.
१९. स्थानांगवृत्ति पृ० २९४, २९५.
२०. बृहत्कल्पभाष्य भाग २, १।१५३९-४०.
२१. आचारांग सूत्र २।३।१।४६५.
२२. कल्पसूत्र-कल्पलता पं० ३।१. तथा कल्पसमर्थनम् गाथा २६.
२३. भ० आ० वि० टीका ४२१, अनगार धर्मामृत ज्ञानदीपिका ९।८०-८१ पृ० ६८९.
२४. ठाणं ५।१०. पृष्ठ ५७५.
२५. वही ५।९९ पृष्ठ ५७४.
संपर्क :
प्रो(डॉ) फूलचंद जैन प्रेमी
(राष्ट्रपति सम्मानित)
अनेकांत- विद्या - भवनम् ,
B23/45,P-6,शारदा नगर,खोजवां,वाराणसी - 221010
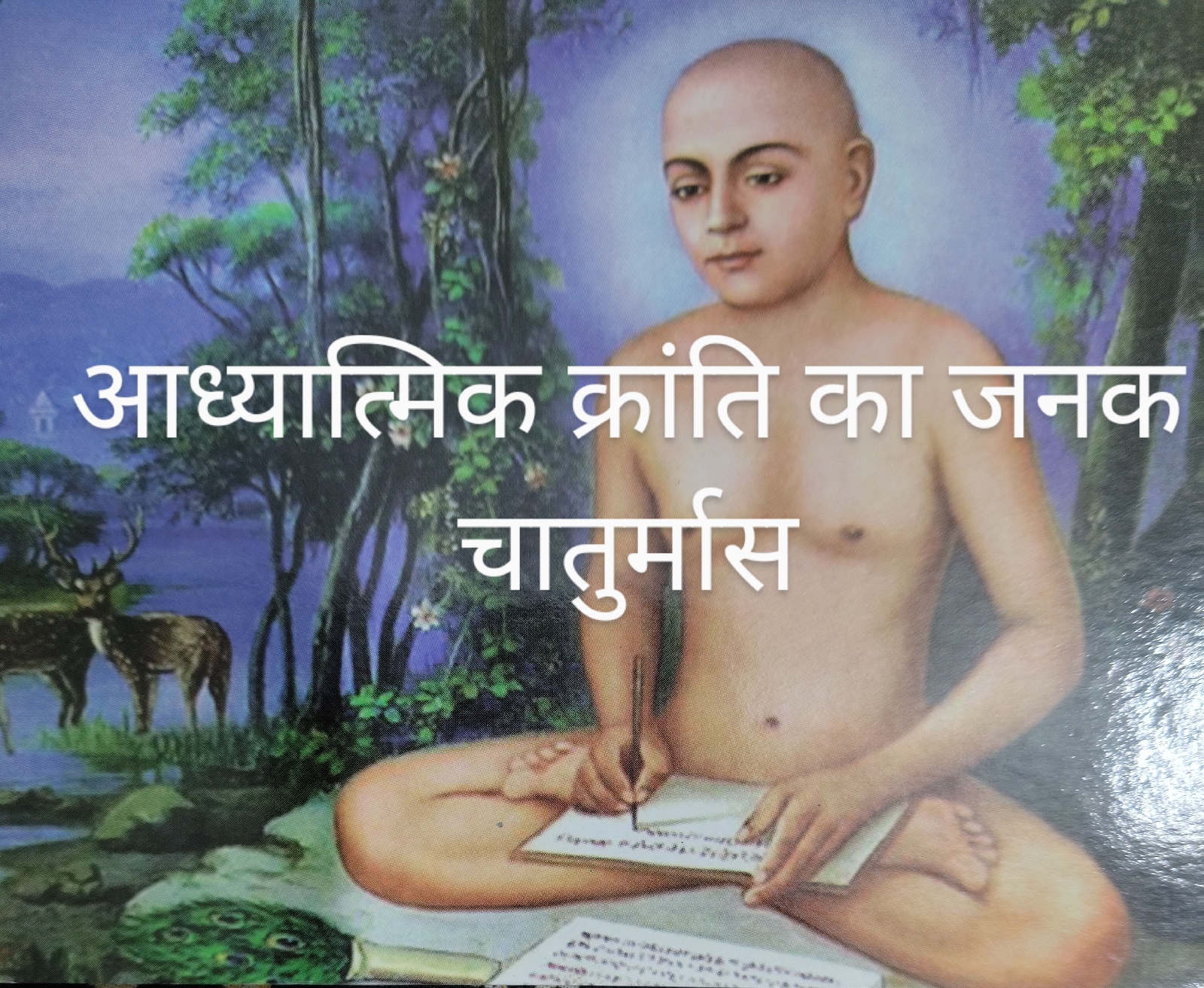

Comments
Post a Comment